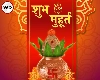कुंभ मेला, शताध्यायी के संदर्भों में त्रिवेणी और तीर्थराज प्रयाग

अनेक पौराणिक आख्यानों के अनुसार प्रयाग को तीर्थराज के रूप में महिमामण्डित किया गया है। वस्तुतः पद्मपुराण के पाताल खण्ड के संवर्ग प्रयाग महात्म्य के सौ अध्यायों के संकलन शताध्यायी में प्रयाग को तीर्थराज कहे जाने के संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक उल्लेख मिलते हैं।शताध्यायी के अनुसार एक बार ब्रह्माजी के पुत्रों ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बहुनेत्रधारी शेषनागजी से प्रयाग के संदर्भ में जानने के लिए निवेदन किया। प्रत्युत्तर में शेषनागजी ने बताया कि तीर्थों में प्रयाग श्रेष्ठतम है।यद्यपि तीर्थ दो प्रकार के होते हैं- एक कामना को पूर्ण करने वाला तो दूसरा मुक्ति प्रदान करने वाला, किन्तु जिस तीर्थ में सभी प्रकार की शक्ति सामर्थ्य हो और वह सबके मनोरथ पूर्ण कर सके अर्थात उस तीर्थ में कामना और मोक्ष, दोनों का मार्ग प्रशस्त हो सके, ऐसा तीर्थ एकमात्र प्रयागराज ही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सारे ही प्रकार के फल देने में समर्थ तीर्थराज प्रयाग ही है।शताध्यायी के ही नौवें अध्याय के अनुसार ब्रह्माजी द्वारा प्रयाग में यज्ञ संपादित करने के बाद जब माधव, नृत्य करते हुए शिव के पास जाते हैं तो देखते हैं कि शिव स्वयं ही माधव-माधव की रट लगाए हुए हैं।अक्षयवट के समीप शिव स्वयं ही बड़े वेग से ताण्डव नृत्य द्वारा वेणी माधव को प्रसन्न करते हैं। त्रिदेवों की ऐसी अद्वितीय एकता मात्र त्रिवेणी में ही साकार रूप ले सकी है। माधव और शिव दोनों ही के द्वारा नृत्य करते हुए एक-दूसरे की आराधना करने के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं।दूसरी ओर प्रणव ध्वनि को त्रिवेणी के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसी क्रम में परब्रह्म वाचक ॐ की मात्रात्मक त्रिधा संगति भी प्रदर्शित की गई है।अकारः शारदा प्रोक्ता प्रद्युम्नस्तत्र देवता।उकारो यमुना प्रोक्ता निरुद्धस्तज्जलात्मकः॥मकरो जाह्नवी गंगा तत्र संकर्षणो हरिः।एवं त्रिवेणी विख्याता वेदबीजं निरूपिता॥महात्म्य की यह अद्भुत कल्पनाहै। एक ओर वेदबीज 'ॐ' तो दूसरी ओर जलमयी त्रिवेणी के वेदोपम रूप। वस्तुतः शताध्यायी ने त्रिवेणी की त्रिगुणात्मिका रूप में कल्पना की है इसीलिए सरस्वती को अरुणवर्णा निरूपित किया गया है।गंगोदभेद तीर्थः गंगा-यमुना के बीच विभेद और समन्वय-भावनाजब प्रयाग में आकर भगीरथी (गंगा) यमुना में मिली तो गंगा से पुरातन नदी होकर भी यमुना ने गंगा को अर्ध्य प्रदान किया जिसे गंगा ने स्वीकार नहीं किया। तब यमुना को संदेह हुआ। उसने कहा- 'गंगे! तुम पूज्य हो, फिर किस कारण मेरा दिया हुआ अर्ध्य नहीं लेती हो, इस विषय में जो तुम्हारा मत हो वह कहो।'गंगा बोली, 'तुम नदियों में बड़ी हो, इसलिए तुममे मिलने से मेरा नाम नष्ट हो जाएगा। यमुने! तुम्हारे साथ से भी यदि मेरा नाम बना रहे तब मैं तुम्हारा दिया हुआ अर्ध्य ग्रहण करूंगी।'यमुना बोली 'सौ योजन तक तुम्हारा ही नाम रहेगा। इसके आगे तुम अलग होकर जाना।' यहां यमुना से पूछ कर गंगा अलग हो गई और प्रसन्नतापूर्वक समुद्र में मिल गई। जिस स्थान में इन दोनों नदियों की धारा अलग हुई है उसको 'गंगोद्भेद' कहते हैं। वह पवित्र तीर्थ है। यहां से सौ धाराओं में होकर यमुना समुद्र में मिली और हजार धाराओं में गंगा समुद्र में मिली।शताध्यायी में यह विवरण उत्तरार्द्ध, अध्याय 272 में श्लोक 40 से 50 तक दृष्टव्य है। भारतीय पुराण कल्पना मानवीय भावों को जड़ चेतन तक व्याप्त करती हुई जिस लालित्य का सृजन करती है वह मुझे बहुत रोचक लगता है। संस्कृति की पहचान इन्हीं मौलिक कल्पनाओं से होती है।जहां सामान्यतया मानव-बुद्धि नहीं जाती वहां यह पुराणकार अपनी प्रतिभा से नए संदर्भ जोड़कर चित्रमाला को पूर्ण कर देते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जो तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें भी पुराणकार स्मरणीय और ग्राह्म बनाकर लोकप्रियता प्रदान कर देते हैं। कल्पित प्रश्न और वैसे ही कल्पित उत्तर इतने विश्वसनीय बना दिए जाते हैं कि लोकमानस उन्हें इतिहास की तरह जानने लगता है। विसंगति यहीं होती है जहां स्वार्थपरता आत्माघाती मनोवृत्ति को प्रश्रय देने लगती है।-
वेबदुनिया संदर्भ