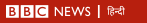दीपक मंडल, बीबीसी संवाददाता
G-20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की तैयारी तेज हो गई है। मीडिया ख़बरों में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत में नौ और दस सितंबर को होने वाले जी-20 सम्मेलन के आखिर में इसका एलान हो सकता है। G-20 सम्मेलन से पहले घोषणापत्र पर काम कर रहे सदस्य देशों के शेरपाओं की बैठक में इस पर चर्चा हुई है।
अगर नई दिल्ली में आयोजित जी-20 सम्मेलन में 55 देशों के संघ अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन की सदस्यता मिल जाती है तो ये ‘ग्लोबल साउथ’ का नेतृत्व करने की भारत की महत्वाकांक्षा को नई ताकत दे सकती है।
भारत इस बात का श्रेय ले सकता है कि उसकी मेजबानी में हुए जी-20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को जी-20 की सदस्यता दी गई।
55 देशों के अफ्रीकी देशों के संगठन अफ्रीकन यूनियन को जी-20 की सदस्यता दिलाने की कोशिश को भारत और चीन के बीच 'ग्लोबल साउथ' का नेता बनने की होड़ के तौर पर भी देखा जा रहा है।
यही वजह है कि चीन ये दावा कर रहा है कि सबसे पहले उसने अफ्रीकन यूनियन को जी-20 में शामिल करने की मांग उठाई थी। रूस भी अफ्रीकन यूनियन को जी-20 में शामिल करने का श्रेय लेना चाहता है।
रूसी मीडिया में रूस के जी-20 शेरपा के हवाले से कहा गया है कि उनका देश इस मांग को उठाने वाले शुरुआती देशों में शामिल रहा है।
भारत या चीन, ग्लोबल साउथ का नेता कौन?
मोटे तौर पर भारत, चीन, ब्राज़ील और अफ्रीका को को ‘ग्लोबल साउथ’ कहा जाता है। ये कोई भौगोलिक विभाजन नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड भी दक्षिणी गोलार्ध में हैं लेकिन ये देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं हैं।
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक काउंसिल फॉर स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस रिसर्च के फाउंडर हैप्पीमोन जैकब के मुताबिक़ ग्लोबल साउथ एक भौगोलिक, भू-राजनैतिक और विकास से जुड़ा पहलू है। हालांकि इस अवधारणा के कुछ अपवाद भी हैं।
ग्लोबल साउथ का नेता बनने के लिए चीन और भारत में एक होड़ चल रही है।अफ्रीकन यूनियन को जी-20 में शामिल कराने की कोशिश का श्रेय लेने की होड़ इस बात का सुबूत है कि ये मुकाबला कितना कड़ा है।
दरअसल भारत को आजादी लगभग उसी समय मिली, जब नए चीन का उदय हो रहा था। लेकिन भारत और चीन की विदेश नीति में अंतर रहा है।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और चीनी मामलों के विशेष अरविंद येलेरी बीबीसी हिंदी से बातचीत में कहते हैं, ''भारत की विदेश नीति समावेशी रही है। वहीं चीन की विदेश नीति में बड़े-छोटे का भाव रहा है। गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन से लेकर सार्क जैसे संगठन भारत की इस नीति के सुबूत हैं। लेकिन चीन ऐसे संगठनों से दूर रहा।''
वो कहते हैं,''अब जबकि चीन को लग रहा है कि वो ‘ग्लोबल साउथ’ यानी विकासशील और कम विकसित देशों का नेतृत्व कर सकता है तो उसके सामने भारत सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उभर चुका है। यही वजह है कि वो ये नेतृत्व हासिल करने के लिए अपनी नीतियों को बदलने की कोशिश कर रहा है।''
अफ्रीका में भारत और चीन की होड़?
विशेषज्ञों का कहना है कि अफ्रीका में भारत चीन से पहले से मौजूद है।
भारत की मौजूदगी वहां सिर्फ निवेश करने या वहां के संसाधनों के दोहन के लिए नहीं है। जबकि चीनी वहां अपने कारोबारी लक्ष्यों के लिए हैं। वो वहां निवेश कर रहा है। वहां के एनर्जी स्रोतों पर उसकी नजर है। वो चाहता है कि ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे अफ्रीका मुहैया करा सकता है, उसका इस्तेमाल अपने हक में करे।
चीन ब्रिक्स सम्मेलन से पहले और इसके बाद भी ये कहता रहा है चूंकि वो अफ्रीका में सबसे ज्यादा निवेश करता रहा है इसलिए उसका सबसे अच्छा दोस्त है। लिहाजा अफ्रीका को जी-20 में लाने का श्रेय उसे मिले। येलेरी की नज़र में चीन को ये श्रेय लेने का हक नहीं है।
वो कहते हैं,''भारत ने चीन से बहुत पहले अफ्रीका में अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाना शुरू कर दिया था।ये कहना बिल्कुल गलत है कि अफ्रीका को अंतरराष्ट्रीय संबंध की मुख्यधारा में लाने का श्रेय अफ्रीका को जाता है। भारत का अफ्रीका से संबंध भू-राजनैतिक नहीं है। जबकि चीन का संबंध भू-राजनैतिक है।''
भारत ने अफ्रीका में 1950, 60 और 70 के दशक में अपने संबंधों को बेहतर बनाने में निवेश शुरू कर दिया था। लेकिन इस दौरान चीन का रवैया वहां मौकापरस्ती का रहा।
येलेरी कहते हैं, "लेकिन जब बाद में जब पता चला कि वहां भरपूर प्राकृतिक संसाधन है तो चीन ने वहां तेजी से निवेश शुरू कर दिया।''
''जबकि भारत ने वहां जमीनी तौर पर काम किया और उसे हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने साझीदार और सहयोगी के तौर पर देखा है। घाना, तंजानिया, कोंगो, तंजानिया और नाइजीरिया जैसे देशों में भारतीय पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन आपको इन देशों में चीनियों के रहने का इतना पुराना इतिहास नहीं मिलेगा।''
येलेरी कहते हैं,''चीन को लगता है कि अगर चीन अफ्रीकी देशों का झंडा अपने कंधे पर लेकर चलेगा तो ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है। यही वजह है कि वो अफ्रीका को साथ लेने की कोशिशों पर दावेदारी जता रहा है।''
भारत को जापान का समर्थन
भारत के अंग्रेजी अख़बार ‘द हिंदू’ ने सामरिक मामलों के एक प्रमुख जापानी टिप्पणीकार के हवाले से लिखा है कि जापान चीन की तुलना में भारत को ग्लोबल साउथ की कमान संभाले देखना चाहता है।
जापान को लगता है कि उसके लिए पश्चिमी देशों को ग्लोबल साउथ के देशों से जोड़ने में चीन की तुलना में भारत ज्यादा मुफीद रहेगा। भारत के प्रति जापान का समर्थन इससे जाहिर होता है कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने मई में हुई जी-7 की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर हिरोशिमा बुलाया था।
येलेरी कहते हैं,''जापान भी अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अफ्रीका में जापान की आर्थिक मदद लगातार बढ़ी है। भारत की अफ्रीका में जापान की तुलना में पहुंच ज्यादा है। भारत में लोकतंत्र है और जापान ऐसे ही देश के साथ अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। जापान की नज़र में अफ्रीका में चीन का रवैया अस्थिर और लेनदेन वाला है। ऐतिहासिक तौर पर भी देखें तो जापान का चीन पर ज्यादा विश्वास नहीं रहा है। इसलिए भी अफ्रीका में जापान भारत के साथ मिल कर काम करना चाहता है।''
येलेरी कहते हैं अफ्रीकी देश अब काफी हद तक नस्लवाद की छाया से बाहर आ चुके हैं। अब वो चाहते हैं उनके यहां लोकतंत्र फले-फूले। लेकिन चीन को लेकर आशंका है। इन देशों में चीन मदद के लिए तो आ रहे हैं लेकिन वो लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन नहीं कर रहा है। लिहाजा अफ्रीकी देशों को अब धीरे-धीरे समझ आ रहा है कि चीन की ओर ज्यादा झुकाव उनके यहां लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है।
अफ्रीका में यूरोप की छाया बनाम एशिया का आकर्षण
येलेरी के मुताबिक़ अफ्रीका में कई देशों में अभी भी उपनिवेश की छाया है। इसलिए इन देशों में ज्यादा विकास नहीं हुआ है। अफ्रीका का अंतरराष्ट्रीय संबंध यूरोप केंद्रित रहा है। लिहाजा यूरोप और अमेरिका अभी भी उन देशों को अपने ऊपर निर्भर देखना चाहते हैं।
वो कहते हैं,''अफ्रीकी देश अब इटली, फ्रांस और जर्मनी देशों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। उनका झुकाव अब भारत, चीन और जापान जैसे एशियाई देशों की ओर बढ़ रहा है। अब मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस जैसे आसियान देश भी अफ्रीका में दिलचस्पी ले रहे हैं।
येलेरी कहते हैं, "अफ्रीकी देशों की एशिया के साथ सांस्कृतिक समानता है। जबकि यूरोपीय देश वहां हमेशा से ही सोना, हीरा बहुमूल्य धातुओं, पेट्रोल और लकड़ी के लिए जाते रहे हैं। विकास के लिहाज से देखें तो तो अफ्रीकी देश 50 साल में यूरोप नहीं बन सकते। 50 साल में वे थाईलैंड बन सकते हैं। 75 साल में मलयेशिया बन सकते हैं। 100 साल में भारत बन सकते हैं। 150 साल में चीन बन सकते हैं। यूरोप बनने में शायद उन्हें 200 साल लग जाएंगे।''