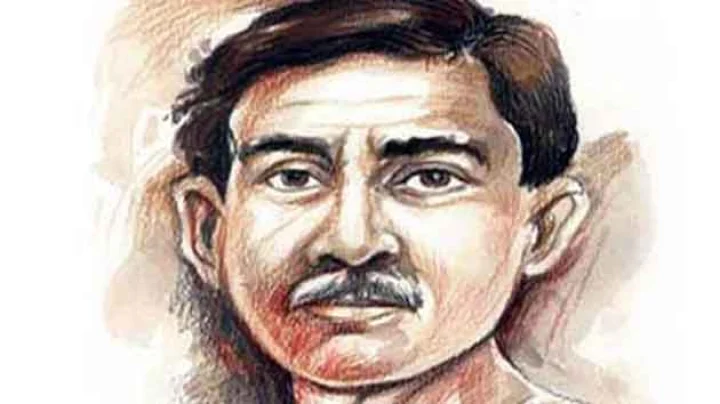मुंशी प्रेमचंद : 'कर्मभूमि' कागज, 'रंगभूमि' कैनवास
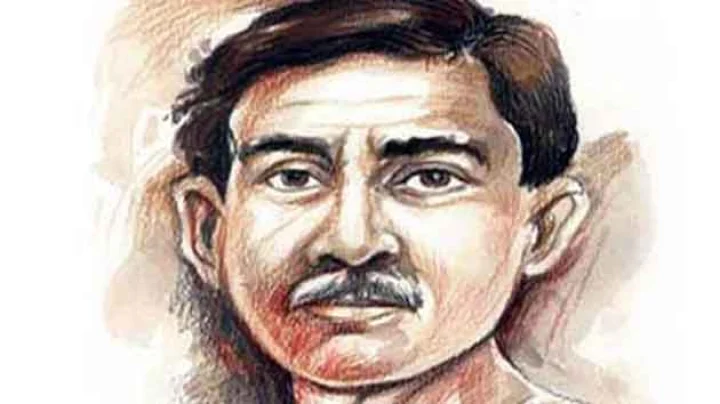
- जितेंद्र वेद
एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए 'कर्मभूमि' कागज थी, तो 'रंगभूमि' कैनवास। इन कागजों के कैनवास पर युद्ध करते-करते न जाने कितनी 'निर्मला' उन्होंने रंग दीं। इस रंग भरने की कोशिश के दौरान उन्होंने कभी भी शब्दों का 'गबन' नहीं किया-जो भी लिखा बिना लाग-लपेट के।
सामाजिक वैषम्यताओं, आर्थिक मुश्किलों, दैहिक आवश्यकताओं को तार-तार करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनके लिए शब्द दान 'गोदान' भी था और महाभोज भी। 1880 से लेकर 1936 यानी 56 साल की अवधि के दौरान उन्होंने साहित्य की यह 'सेवा' -विपन्नताओं,तकलीफों, वैषम्यताओं तथा देश, काल व समाज की अन्य मुश्किलों के 'सदन' में रहकर।
साहित्य समाज का दर्पण होता है और स्व का चित्रण भी। व्यक्ति जितना भोगता है, जितना सहन करता है, जिसका प्रत्यक्ष गवाह होता है वह गाहे-बगाहे अपनी कलम के माध्यम से पाठकों के सामने परोस देता है। इस थाली में परोसे गए भोज्य पदार्थ में साहित्यकार की संवेदना, अंतर्वेदना, मनोवेदना का वही अनुपात-समानुपात होता है, जो हम दैनिक जीवन में हम देखते हैं, भोगते हैं, निरपेक्ष भाव से ग्रहण कर लेते हैं। फिर किसी भी समाज में दुख का अनुपात सुख को हमेशा मात देता है तो साहित्य भी कैसे अछूता रह सकता है।
इस 'कलम के सिपाही' में ये सब भावनाएँ कूट-कूट कर भरी हुई थी। प्रेमचंद ने अपनी संवेदनाएं, होरी-धनिया, गोबर-झुनिया, अमरकांत, सूरदास आदि के माध्यम से व्यक्त की है। असहनीय गरीबी के लम्हों को बिल्कुल ठंडे दिमाग से झेलने की क्षमता, चट्टानों से बिना आपा खोये निपटने की जिजीविषा हममें आदरभाव भर देती है। दूसरी ओर मातादीन जैसे पात्र को समझने पर हमारे मन में उपेक्षा भाव ज्यादा होता है, घृणा भाव कम।
हर समाज अच्छे-बुरे का हेट्रोजीनियस (विषमांगी) मिश्रण होता है। बुरा कितना भी बुरा क्यों न हो - वह घृणित नहीं होता है। वह किसी भी समाज की आवश्यक बुराई की तरह होता है, इसलिए उसे वैसा ही स्वीकार करने की कला सुझाने का श्रेय मुंशी प्रेमचंद को जाता है। दरअसल प्रेमचंद के बारे में लिखते समय एक कहानी का नाम लिखो तो यकायक जेहन में दूसरा नाम आ जाता है।