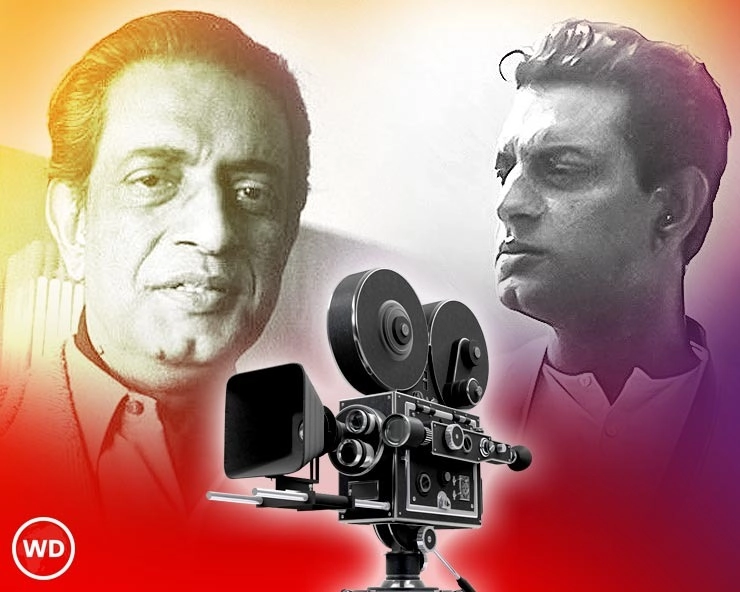सत्यजीत रे आज हमारे बीच होते तो 2 मई 2021 को उम्र के सौ बरस पूरे कर लेते। सिनेमा अगर जीवन की विस्तारित छवि है, तो कभी-कभी फिल्मकार इस विस्तार से भी पार खड़ा नजर आता है। विश्व सिने इतिहासमें ऐसा कम ही हुआ है, जब किसी सिने शिल्पी का कद रजतपट को एक विराट अनुभव से भर पाया। भारत में यह खगोलशास्त्रीय घटना तब घटी, जब सत्यजीत रे जैसे धूमकेतु ने सिने आकाश को अपनी अद्वितीय प्रतिभा के आभामंडल से स्पंदित किया।
वस्तुगत और विषयगत दोनों लिहाज से इस महान फिल्मकार के अप्रतिम व्यक्तित्व का कोई सानी नहीं है। एक सिनेकर्मी की नजर से उनकी समग्र दृष्टि मानवमात्र के जीवन संघर्ष के असमतल किनारों को छूती है, वहीं अपने जीनियस के अविश्वसनीय विस्तार से वे साधारण मनुष्य सीमित रचनात्मक परिधि को बेहद छोटा बना देता हैं। यह महामानवीय व्यक्तित्व ही रे की सबसे बड़ी पूंजी कही जाएगी। पचास के दशक में एक फिल्म को कान फिल्मोत्सव में मानवता का उत्कृष्टतम दस्तावेज करार दिया गया। सिने आस्वाद के क्षेत्र यह अनूठी क्रांति का सूत्रपात था। पहली बार किसी भारतीय सिनेकर्मी की फिल्म पश्चिमी समालोचकों द्वारा इस कदर सराही गई। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता/निर्देशक जॉन हस्टन, जो उन दिनों रूडयार्ड किपलिंग के उपन्यास ‘द मैन हू वांटेड टू बी ए किंग’ को फिल्माने भारत आए हुए थे, वे इस फिल्म को देखकर बोले- ‘यह सिनेकर्म का सर्वथा अभिनव अंदाज है।‘ यह फिल्म थी ‘पाथेर पांचाली’ (1955) और इसके निर्देशक थे सत्यजीत राय। कोलकाता के ऑर्डिनेस छबिगृह में प्रदर्शित होने से पूर्व इसका सार्वजनिक प्रदर्शन न्यूयॉर्क के दर्शकों के लिए किया जा चुका था। फिल्म जब दिल्ली के डिलाइट सिनेमाघर में प्रदर्शित की गई, तो गैर बंगाली दर्शकों ने महज चाक्षुष आकर्षण के चलते जमकर सराहा। यह चर्चा आग की तरह कला जगत में फैल चुकी थी कि ऐसी पहली फिल्म कभी नहीं बनी। सिर्फ चौबीस वर्ष के एक युवा सिनेकर्मी ने ऐसी फिल्म बनाकर समीक्षकों को हैरान कर दिया था, जिसमें पारंपरिक फिल्मांकन से अलग अनूठे आशय मौजूद थे। बिमल राय की ‘दो बीघा जमीन’ जैसे अपवाद छोड़कर ज्यादातर भारतीय फिल्में स्टूडियो की चहारदीवारी में फिल्माई जाती थी। ‘पाथेर पांचाली’ ने लोकेशन शूटिंग की महत्ता अपने विशिष्ट अंदाज में स्थापित की। कई मायनों में इस फिल्म ने मिथकीय और अतिरंजनाप्रधान हिन्दी सिनेमा के प्रारूप तोड़कर नई भंगिमाओं की तलाश की।
राय-ऋषि
अगर भारतीय सिनेमा के विकास की महागाथा लिखी जाए, तो सत्यजीत राय नि:संदेह एक ऋषि की हैसियत से नवोन्मेषी शोधकर्ता की श्रेणी में रखे जाएंगे। रे के परिदृश्य पर उभरने तक हिन्दुस्तानी सिनेमा रंगमंच के अतिनाटकीय प्रभाव की गिरफ्त में पूरी तरह घिरा हुआ था। रे ने बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय की कहानी पर ‘पाथेर पांचाली’/ ‘अपराजितो’/ ‘अपूर संसार’ जैसी फिल्में बनाकर सिनेकर्म को एक नई दिशा दी। राय का सिनेमा फंतासी का रचनालोक न होकर यथार्थवाद की ओर करवट लेता है। इसके बावजूद उनकी फिल्मों में कहीं राजनीतिक मंतव्य नहीं है। प्रतिद्वंद्वी और सीमाबद्ध जैसी फिल्मों में युवा हताशा को रेखांकित करते हुए भी वे कला और सरोकार की अर्थहीन बहस में नहीं पड़ना चाहते। स्वयं उनके शब्दों में, ‘लोग मुझे गैर प्रतिबद्ध फिल्मकार कहते हैं। आखिर यह है क्या बला? मैं मानवमात्र के लिए समर्पित हूं। मेरे लिए यही पर्याप्त है।‘ रे की फिल्में अपने समूचे देशज स्वरूप में मनुष्यत्व की तलाश करती हैं, बौद्धिकता के परचम नहीं लहरातीं। रे की फिल्मों का हर दृश्य एक किताब की तरह पढ़ा जा सकता है। स्वयं एक उच्चस्तरीय चित्रकार होने के नाते वे हर दृश्य की रूपरेखा कागज पर रेखांकित करने के लिए विख्यात थे। साहित्य और सिनेमा के अंतर्संबंध पर उनकी राय थी कि हर किताब फिल्मांकन के लिए नहीं होती। यदि ऐसा होता तो हर पृष्ठ एक दृश्य की तरह लिखा जाता और तब हम से उत्कृष्ट साहित्य का दर्जा नहीं देते। इसके विपरीत रे ने अपनी कृतियों के हर दृश्य को एक पाठ्यपुस्तक की शक्ल में ढाला, इसीलिए आज भी सिने अध्येता उनके दृश्य विवरण को विश्लेषण की कसौटी पर रखते हैं। मिसाल के तौर पर ‘अपराजितो’ में बनारस के घाट और अपु की पिता की मृत्यु पर उड़ते कबूतरों का फिल्मांकन। शायद ऐसे ही अद्भु त निर्देशकीय कौशल की वजह से जापानी फिल्मकार अकीरा कुरोसावा ने रे के बारे में कहा था कि इस अविश्वसनीय सृजनशैली के चलते सिनेप्रेमी उन्हें हर युग में नए सिरे से खोजने की कोशिश करेंगे। रे के लिए प्रतीकात्मक फिल्मांकन से कहीं ज्यादा महत्व जीवन की पल-पल बदलती स्थितियों के विश्लेषण का था। फिल्म ‘जलसाघर’ में रूपकों के एकाधिक प्रयोग को लेकर वे सहज नहीं थे। जाहिर तौर पर जो लोग उनके सिनेमा को जटिल या अतिबौद्धिक करार देते हैं, दरअसल उन्हें समझना चाहिए कि रे ने कभी अपनी फिल्मों में विचारधारा का आरोपण नहीं किया।

गुरुदेव-गाथा
अपने चार दशकीय करियर में रे ने तीस फिल्मों और पांच वृत्तचित्रों का निर्माण किया। उनकी आखिरी फिल्म आगंतुक (1991) में प्रदर्शित हुई थी। एक प्रकार से रे की फिल्में बंगाल पुनर्जागरण के उस दौर की प्रतिनिधि कृतियां कहीं जा सकती हैं, जिसके वे आखिरी उत्तराधिकारी माने जाते थे। रे का रचना संसार बांग्ला परिवेश तक सीमित रहा, पर उनकी फिल्में समूची मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। एक पश्चिमी समालोचक ने उनकी फिल्मों को ऐसे भूदृश्य की संज्ञा दी थी, जो अपनी गहन खामोश उपस्थिति से सभ्यता को सोचने का एक नया अंदाज देती हैं। कला परिदृश्य पर रे के उभरने तक बंगाल उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। बांग्ला-साहित्य के प्रति अगाध प्रेम के चलते रे ने सिर्फ दो हिन्दी फिल्मों ‘सद्ग-ति’ और ‘शतरंज के खिलाड़ी’ के लिए प्रेमचंद की रचनाओं का सहारा लिया। ई.एम. फॉर्स्टर के मशहूर उपन्यास ‘ए पैसेज टू इंडिया’ पर भी वे फिल्म बनाना चाहते थे। इसके मुस्लिम रुझान वाले परिवेश में कुछ तब्दीली का इरादा भी उन्होंने बना रखा था। वह फिल्म नहीं बन पाई। मुंबइया सुपर स्टार अमिताभ के साथ फिल्म निर्माण की योजना को भी रे मूर्तरूप नहीं दे सके। दरअसल गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं का इतना गहरा प्रभाव रे पर रहा कि इस बाग से बाहर जाने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। टैगोर की कहानियों पर रे ने ‘तीन कन्या’ और ‘चारुलता’ जैसी फिल्मों का निर्माण किया। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर (टैगोर) से रे की पहली मुलाकात 1928 में तब हुई थी, जब वे सात वर्ष के थे। अपनी मां के साथ रे टैगोर विश्वविद्यालय पहुंचे, तो उनकी मां ने गुरुदेव के आगे एक पुस्तिका रखकर कहा- ‘आप मेरे बेटे के लिए इस पर कुछ लिखें।‘ गुरुदेव ने लिखा- ‘मैंने दुनियाभर में घूमकर पर्वतों और नदियों को देखने में अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी। मैं सिर्फ अपने घर के पास घास के उस नन्हे तिनके पर पड़ी ओस की वह चमकती बूंद नहीं देख पाया, जो अपने आप में पूरा ब्रह्मांड समेटे थी।‘ रे के अनुसार यह उद्गार उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त करता रहा। रे का रचनाकर्म विश्वबंधुत्व और अंतराष्ट्रीय सरोकार के कागजी नारों में पड़ने के बजाय घास के तिनके पर मौजूद ओस की बूंद को परखने का प्रयास करता रहा है, जहां जीवन अपनी उद्याम जिजीविषा के साथ महक रहा है। रे की फिल्में एक ओर जहां अपनी मर्मस्पर्शी कथ्यशैली से दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती हैं, वहीं प्रस्तुति के स्तर पर उनमें गहरा आनंद भी है। मिसाल के तौर पर ‘पाथेर पांचाली’ में अपु के बालपन और गांव में आए लोकनाट्य का मंचन देखते हुए उसकी उल्लसित भंगिमा जीवन को अपने निश्छल स्वरूप में पेश करती है। ‘गूपी गाइने बाघा बाइने’/ सोनार किला/ जय बाबा फेलुनाथ/ हीरक राजार देशे जैसी फिल्मों में रे ने बाल अवचेतन में झांकते हुए जिंदगी की जीत के रूपवादी लक्ष्य को साधा है। एक फिल्मकार के बतौर उनके कृतित्व की परिधि इतनी विस्तृत है कि उनमें कुछ भी अछूता नहीं रह जाता।
सूक्ष्मदर्शी अवलोकन
रे की जीवनचर्या में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चीजों का लघु विश्लेषण करना भी शामिल रहा। कोशिकाओं के स्तर पर घटित होती जीवन की लय पर आंखें गड़ाए रे अपनी फिल्मों में इतनी बारीक और गहन अंतर्दृष्टि बरकरार रख पाए। उनकी फिल्मों के सर्वजनीन और सर्वकालिक स्वरूप का प्रमाण यह कि अंगरेजी भाषी पश्चिमी दर्शकों और समालोचकों ने उन्हें सर्वाधिक सराहा। मजे की बात है कि ‘तीन कन्या’ को छोड़कर उनकी कोई भी फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षकों के साथ प्रदर्शित नहीं हुई थी। सिर्फ कापुरुष-ओ-महापुरुष (1965) हिन्दी उपशीर्षक के साथ जारी हुई। इसके बावजूद बांग्ला दर्शकों से इतर वैश्विक दर्शक वर्ग उनके रचनाकर्म की ऊंचाई को बयान कर देता है। रे की फिल्में अपने विजुअल इम्पेक्ट (दृश्य प्रभाव) के लिए इतनी प्रभावशाली है कि भाषा और राष्ट्रीयता की सीमाएं वहां गौण हो जाती हैं। सही अर्थ में रे के जरिये ही भारतीय सिनेमा एक वैश्विक स्वरूप ले पाया। सिने हलकों में यह बात प्रचलित रही कि दुनिया दो हिस्सों के बीच बंटी है- एक वह लोग जो रे की फिल्में देखते हैं और दूसरे जो नहीं देखते। सर्वहारा-पूंजीपति, पाश्चात्य-पूर्व, आस्तिक-नास्तिक से परे यह जगत का अनूठा वर्गीकरण था। इसके बाद भी रे के आलोचकों की संख्या कम नहीं रही। ‘कंचनजंघा’ (1962) के प्रदर्शन पर एक समीक्षक ने इसे एंटी फिल्म करार देते हुए इसकी खिल्ली उड़ाई, वहीं वामपंथी सोच के कुछ समालोचकों ने रे को अपनी फिल्मों में वर्ग-संघर्ष के अभाव का भी दोषी ठहराया। रे ने इसका जवाब देते हुए स्पष्ट किया था कि वे मनुष्य को राजनीतिक संवेगों के आधार पर वर्गीकृत करने के बजाय उसका मनोसामाजिक विश्लेषण करना जरूरी समझते हैं। शेक्सपियर और एडोल्स हक्स्ले जैसे लेखकों और विटोरियो द सीका, रोजेलिनी, फेडरिको फेलिनी जैसे निर्देशकों से प्रभावित होकर रे ने अपनी निर्देशकीय यात्रा का जो मार्ग चुना था, उसमें टकराव के लिए कोई जगह नहीं था। शायद यही वजह है कि रे की फिल्में (यहां तक की प्रतिद्वंद्वी भी) हिंसक संघर्ष को गैर जरूरी करार देती हैं। चिरंतन भारतीयता का दार्शनिक स्वरूप उनकी फिल्मों का केन्द्रीय सूत्र है, जो यथार्थ की अनूठी मंजूषा सिनेकर्म की शक्ल में पेश करता है। उनकी तमाम फिल्मों में पारंपरिक भारतीय चिन्हों का रूपांकन साफ नजर आता है। देवी (1960) जैसी फिल्म में जहां एक नव-विवाहित (शर्मिला) अपने श्वसुर द्वारा दुर्गा प्रतीक मान ली जाती है, रे किसी निश्छल विश्वास को अंधविश्वास बताकर उसका मखौल उड़ाते नजर नहीं आते। रे का कैमरा एक ऐसा सूचक है, जिस पर जीवन के स्पंदन पूरी शिद्दत से लिपिबद्ध होते चले जाते हैं, बगैर किसी पक्ष-विपक्ष के। शायद इसी वजह से उनके आलोचक उनकी फिल्मों को डॉक्यूमेंट्री सिनेमा भी करार देते हैं। मगर यह टीका उतनी सीमित है, जितनी रे की प्रतिभा का विस्तार असीमित है। समाज के हर वर्ग के जीवन का अंतर्द्वंद्व उनकी फिल्मों में मुखरित होता है। जहां अपु-त्रयी की फिल्में विपन्नता के रचनाशास्त्र को टटोलती हैं, वहीं ‘देवी’ और ‘जलसाघर’ जैसी फिल्मों में रे उच्चवर्गीय सामंत परिवारों के अंत:स्थल को छूते हैं। अभिजात/ महानगर/ सीमाबद्ध/ नायक/ आगंतुक जैसी फिल्मों में रे ने आधुनिक शहरी जनजीवन के स्याह-सफेद पन्नों को पढ़ने की कोशिश की है। रे का सिनेमा पूरी तरह से आग्रह मुक्त सिनेमा है।
पंडितजी का आशीर्वाद
रे के कृतित्व की लंबी यात्रा तब शुरू हुई, जब स्वातंत्र्योत्तर भारत अपने शैशवकाल में था, जाहिर तौर पर आजादी के कुछ महानायक रे के भी पसंदीदा बने। पंडित नेहरू की पाश्चात्य और भारतीय जीवनशैली का सामंजस्य रे को आकर्षित करता रहा। वे स्वयं भी योरप और हिन्दुस्तानियों के कलात्मक समन्यव के प्रतीक कहे जा सकते हैं। नेहरू अपने इस समानधर्मा की फिल्मों के इतने बड़े प्रशंसक थे कि उन्होंने सभी देशों में मौजूद भारतीय दूतावासों को रे की फिल्म ‘पाथेर पांचाली’ प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। स्व. इंदिरा गांधी भी रे की विराट शख्सियत के आगे प्रशंसा के भाव में खड़ी रही। उन्होंने रे के समक्ष पहले एक सामाजिक संदेश प्रधान कृति और फिर अपने पिता पं. नेहरू पर एक फिल्म राजसहायता से बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे रे ने स्वीकार नहीं किया। एक खुद्दार रचनाकर्मी की इस ईमानदारी ने चाटुकारों से अलग श्रीमती गांधी की नजर में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। ‘पाथेर पांचाली’ को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा खरीद जाने के अलावा रे राजसहायता से दूर रहे। डेढ़ लाख की लागत से बनी ‘पाथेर पांचाली’ की शूटिंग के लिए उन्होंने नौ हजार पांच सौ रुपए की अपनी बीमा पॉलिसी और पत्नी के जेवर गिरवी रखकर जुटाए थे। छ: फुट पांच इंच लंबे कद वाला यह फिल्मकार अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से गरिमा के उत्कर्ष का प्रतिबिम्ब झलकाता रहा। रे के विदेशी वितरक एडवर्ड हैरीसन ने सच ही कहा था- ‘हमें रे की फिल्मों की देखभाल नन्हे शिशुओं की तरह करनी चाहिए।‘
फिल्म संस्कृति (2005) : माणिकदा सत्यजीत राय से साभार